गुप्त साम्राज्य का उदय
गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशांबी में हुआ था जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वह है श्री गुप्त हालांकि प्रभावती गुप्त के पुणे ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। यह प्राचीनतम भारतीय साम्राज्य था जो लगभग 319 से 605 ईसवी तक अपनी चरम पर मौजूद था और भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश हिस्सों पर इनका आधिपत्य स्थापित था।मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही कुषाण एवं सात वाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में तीन राजवंशों का उदय हुआ जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी भाग में गुप्त वंश प्रमुख है मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को गुप्त तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी के शुरुआत में हुआ गुप्त वंश का प्रारंभिक राजा आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। श्री ग्रुप में गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्ष बाद किया पुराणों में यह कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा द्रोणी प्रयाग साकेत तथा मगध में फैला था श्री गुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी अतः श्री गुप्त किसी के अधीन शासक था प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार उक्त धाराओं के अधीन छोटे से राज्य प्रशासन चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव को दान दिए थे।

गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोतों में विशाखदत्त खरीद देवीचंद्रगुप्तम तथा मुद्राराक्षस शुद्र का मृच्छकटिकम् कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम् कुमारसंभवम् रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम् प्रमुख है स्मृतियों में बृहस्पति नारद आदि प्रमुख है पुराणों के अनुसार वायु पुराण मत्स्य पुराण विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण आदि से हमें गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है इनके अलावा बौद्ध साहित्य मैं मंजूश्री मूल कल्प तथा वसुबंधु चरित तथा जैन साहित्य जिनसेन रचित हरिवंश पुराण से भी हमें गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है इनके अलावा विदेशी साहित्य को में फाह्यान का फो-क्यों-कि तथा युवान च्वांग ह्वेनसांग का सी-यु-की आदि ग्रंथ प्रमुख है। साथ ही पुरातात्विक स्रोतों से भी इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है यथा प्रशासकीय एवं अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति एवं एरण अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख तथा उदयगिरी गुफा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर लेख गढ़वा शिलालेख दिलशाद स्तंभ लेख स्कंद गुप्त का जूनागढ़ प्रशस्ति भीतरी स्तंभ लेख प्रमुख है।गुप्त साम्राज्य की जानकारी में मुद्राओं का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है गुप्त योग्य से भारतीय मुद्रा के इतिहास में नवीन युग की शुरुआत आती है गुप्त शासकों की स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं मंदिर एवं मूर्तियां उदयगिरि भूमरा नाचना कुठार देवगढ़ एवं तिगवा के मंदिर सारनाथ बुद्ध मूर्ति मथुरा की जैन मूर्तियां अजंता व भाग्य चित्र भूमि अदनान संबंधी भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अतः गुप्त वंश का इतिहास की जानकारी के लिए उपरोक्त स्रोतों का होना अति आवश्यक है।

सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोतों में पुराणों का महत्व पूर्ण स्थान है पुराणों में दी गई वंशावली यों का आलोचनात्मक अध्ययन करने के बाद या निष्कर्ष निकाला गया है कि पुराणों में दी गई गुप्त वंश संबंधी जानकारी विश्वसनीय है पुराणों की संख्या 18 है किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वायु प्रवाह ब्रह्म पुराण मत्स्य पुराण विष्णु पुराण और भागवत पुराण अत्यधिक महत्त्व रखते हैं पुराणों से गुप्त साम्राज्य उसके विभिन्न प्रांतों तथा सीमाएं स्पष्ट चित्र मिलता है साम्राज्य के अखंड भागो तथा उसके कार्य क्षेत्र से बाहर के प्रदेशों में अंतर रखा गया है राजाओं तथा छोटे-छोटे राज्यों के नाम याद करने तथा उनकी क्षमता स्थापित करने में पुराणों से सहायता मिलती है साम्राज्य के अंदर के राज्य तथा स्वतंत्र राज्यों के अभ्युदय का समय निश्चित करने में भी वे सहायक रहे हैं पुराणों से ही ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम साकेत तथा मगध में राज्य करता था गुप्त साम्राज्य के राज्य के पूर्वार्ध में उसके समकालीन शासक को जैसे तथा वाकाटक वंश और सिंध तथा पश्चिमी पंजाब में शक आदि का पूर्ण विवरण पुराणों से प्राप्त होता है।धर्म शास्त्रों से भी बहुत से लाभदायक सामग्री प्राप्त होती है जयसवाल मानता है कि नारद का समय पूर्व गुप्त काल था संभवत बृहस्पति भी पूर्व गुप्त काल में ही जीवित रहा व्यास हरित पितामह की स्मृतियां भी संभवत गुप्त काल में ही लिखी गई थी उनकी रचनाओं से पर्याप्त जानकारी मिलती है। मंदाकिनी 30r की रचना संभवत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उसके प्रधानमंत्री शिखर ने की पुस्तक का उद्देश्य राजा को आदेश देना था लेखक ने अपने स्वामी द्वारा सक शासक के वध की रक्षा की है।

लेखक के शब्दों में भेष बदलकर शत्रु की हत्या करने से नैतिकता का उल्लंघन नहीं होता। काव्य-नाटक साहित्य भी हमारे लिए लाभदायक है सेतुबंध काव्य या सेतु काव्य कौमुदी महोत्सव देवीचंद्रगुप्तम और मुद्राराक्षस इसी श्रेणी में आते हैं। सेतुबंधम एक प्राकृत काव्य है जिसमें लंका पर आराम के आक्रमण तथा रावण के वध को चित्रित किया गया है इस पुस्तक की रचना वाकाटक राजा भंवर सिंह ने की थी कौमुदी महोत्सव 5 अंकों में लिखा गया एक नाटक है कुछ विद्वानों का विचार है कि इस पुस्तक की रचना किशोरी का ने की और कुछ अन्य विद्वानों ने व जी का को इसकी लेखिका बताया है। मगर वास्तविकता यह है कि इस पुस्तक की रचना 340 इसी में की गई और इसमें मदद की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का चित्रण किया गया है इस नाटक की कथा के अनुसार सुंदर वर्मा मगध का राजा था उसकी कई रानियां थी लेकिन उस में से किसी ने भी पुत्र को जन्म नहीं दिया था जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसने चंद्रसेन को दत्तक पुत्र बना लिया वह मदद खुद का था और उसकी पत्नी लिखी हुई जाति की थी प्लीज कोई मदद के राजवंश के पुराने शत्रु थे नाटक में छवियों को मलेज कहा गया है चंद्रसेन को गोद लेने के बाद सुंदर वर्मा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने कल्याण वर्मा रखा राजा अपने पुत्र को बहुत चाहने लगा चंद्रसेन को यह अच्छा ना लगा और उसने अपने पोषक पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया युद्ध में सुंदर वर्मा की मृत्यु हो गई और चंद्र सेन राजा बन गया प्रधानमंत्री मंत्र गुप्त तथा सेनापति कुंजारा को यह मानना था और उन्होंने स्वर्गीय राजा के वास्तविक पुत्र का पक्ष ले लिया उसे बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहां वह कई वर्ष रहा प्रधानमंत्री तथा सेनापति अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जब उसे सिंहासन पर बैठाया जाए सीमांत प्रदेश में एक विद्रोह को दबाने के लिए चंद्रसेन को राजधानी छोड़नी पड़ी चंद्रसेन की अनुपस्थिति में कल्याण वर्मा को राजधानी में लाया गया और चंद्रसेन को गद्दी से उतार कल कल्याण वर्मा को राजा बना दिया गया कहा गया है कि चंद्रसेन ही गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम था इस नाटक में गुप्त वंश की उत्पत्ति तथा उन्नति पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है गुप्त वंश के इतिहास की गई उलझन को सुलझाने में इसने विद्वानों की सहायता की है।
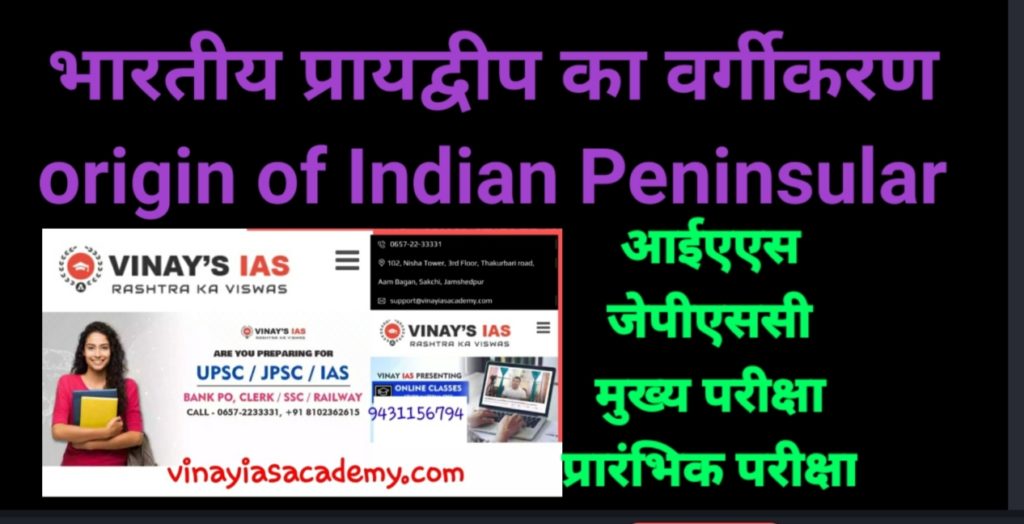
देवीचंद्रगुप्तम एक राजनीतिक नाटक है और इसकी रचना का श्रेय मुद्राराक्षस के लेखक विशाखदत्त को दिया जाता है इस नाटक की पूर्ण प्रति प्राप्त नहीं हो सकी है मगर कुछ लेखकों द्वारा लिए गए उठकर उदाहरण ही प्राप्त हुए हैं अभिनव गुप्त ने इसके उदाहरण अभिनव भारतीय में दिए भोज ने श्रृंगार प्रकाश में रामचंद्र ने न्याय दर्पण में तथा सागर ना दिन ने नाटक लक्षण रत्न कोष में इसके उदाहरण दिया इस पुस्तक में दी गई जानकारी को एकत्र करके देवीचंद्रगुप्तम की पूर्ण प्रति बनाई जा सकती है नाटे दर्पण से ज्ञात होता है कि राम गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था अंत:पुरा में रानी का सेवक माधव सिंह था राजकुमार चंद्रसेन रानी का प्रेमी बन गया सतपति राम गुप्त का शत्रु था उन दोनों के युद्ध में राम गुप्त की पराजय हुई और उसने अपनी रानी ध्रुव देवी को शक राजा को देना स्वीकार किया बताया गया है कि राम ग्रुप में या शक मंत्रियों के परामर्श से स्वीकार की जनता के परामर्श से नहीं।विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस से भी लाभदायक जानकारी मिलती है कथावस्तु तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना से संबंध है किंतु प्रतीत होता है कि विशाखदत्त ने अपने समय में गुप्त वंश की स्थापना संबंधी घटनाओं का उल्लेख भी कर दिया है नाटक कूटनीति तथा राजनीति भरपूर है गुप्त काल में राजा के धर्म तथा जनता की धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक सहिष्णुता प्रचलित थी नाटक में जीव सिद्दीकी महत्वपूर्ण स्थिति से इसकी पुष्टि होती है।
फाहियान एक चीनी यात्री लेखक खा लिया चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था इसके विवरण में गुप्त कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है इसने अपने विवरण में मध्य एशियाई देशों के बारे में बताया है या चीन से रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का समूह था जिसके माध्यम से एशिया यूरोप अफ्रीका जुड़े हुए थे इससे होते हुए भारत आया था।फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षुक यात्री लेखक एवं अनुवादक थे जो 399 ईसवी से लेकर 412 ईसवी तक भारत श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आए उनका दिए यहां से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें वापस छीन ले जाना था उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने पूरे ग्ररंथ में लिखा जिसका नाम बहुत राज्यों का एक अभिलेख चीनी बिच्छू आसियान की बौद्ध अभ्यास पुस्तकों की खोज में भारत और शिलोन की यात्रा था।

उनकी यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था और चीन में जीन राजवंश का काल चल रहा था। फाह्यान द्वारा लिखित विवरण से भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है ।फाहियान का मुख्य उद्देश्य बौद्ध पुस्तकों तथा कि मंत्रियों की खोज करना था किंतु उसने तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति की भी पर्याप्त जानकारी दी उसने नगरों तथा नागरिकों के धन समृद्धि का उल्लेख किया है राज्य तथा अन्य परोपकारी संस्थाओं द्वारा चलाए निशुल्क चिकित्सालय कभी उसने वर्णन किया है। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग का भी इतिहास में नाम उल्लेखनीय है वह भी एक बौद्ध भिक्षुक था यो चीन से सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था उसने वहां के प्रसिद्ध आचार्य से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा सिंह ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मले निकुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है उस समय के भारत पर प्रकाश डाला इस ग्रंथ से हमें उस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं मिलती परंतु जागरण बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास का अमूल्य स्रोत माना जाता है इसने भारत में कागज का प्रयोग देखा था सिंह ने अपनी पुस्तक में जय आदित्य के वृत्तीसूत्र का उल्लेख किया है।चीनी यात्री ईत्सिग ने हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की यात्रा की उसने महाराजा श्री गुप्त का उल्लेख किया है जिसने चीनी तीर्थ यात्रियों द्वारा एक मंदिर निर्माण करवाने का उल्लेख किया है। गुप्त काल की जानकारी में अभिलेखों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है गुप्तकालीन इतिहास लिखने में अभिलेख भी काफी सहायक सिद्ध हुए हैं गुप्त अभिलेखों में आरंभिक गुप्त राजा तथा उनके उत्तराधिकारी ओं के अभिलेख हैं किंतु डॉक्टर फ्लिट ने केवल आरंभिक गुप्ता राजाओं के ही नहीं बल्कि उत्तर कालीन गुप्त राजाओं के अभिलेख भी संकलित किए हैं।आरंभिक गुप्त राजाओं की मुख्य शाखा को स्कंद गुप्त के साथ समाप्त हुई समझा जाता है 484 ईसवी का बुध गुप्त तथा 510 का भानु गुप्त का पर्स के क्रम से 19 तथा 20 अभिलेखों में उल्लिखित है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से भारतीय नेपोलियन की विधियों का विस्तृत विवरण मिलता है समुद्रगुप्त के एरण शिलालेख अभिलेख संख्या 2 से भी समुद्रगुप्त की शक्ति तथा कार्यकलापों का ज्ञान होता है।उदयगिरि गुफा अभिलेख मथुरा शिलालेख सांची शिलालेख और गढ़वा शिलालेख सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं और धर्म के प्रति राज्य की नीति से हमें अवगत कराते हैं गढ़वा शिलालेख मिल चार स्तंभ शिलालेख और मन कुंवर मूर्ति शिलालेख में कुमारगुप्त प्रथम का वर्णन है दो भागों में बिहारी स्तंभ शिलालेख भिकारी स्तंभ शिलालेख जूनागढ़ जिला अभिलेख कहां हो स्तंभ शिलालेख और इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में स्कंद गुप्त का वर्णन दिया गया है।

महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में किसी राजा चंद्र का वर्णन है व्यास नदी के निकट एक पहाड़ी पर इसके मालिक स्थान से दिल्ली का एक शासक इसे दिल्ली के निकट महरौली ले आया इस अभिलेख में कहा गया है कि उसके विरुद्ध संगठित एक राजा समूह के विरुद्ध युद्ध करके उसने वह लिखो पर भी विजय पाई उसने अपनी विजय ख्याति दक्षिणी समुद्र तक पहुंचा ही अपनी भुजाओं की शक्ति से उसने संसार में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित की।स्कंद गुप्त के भी तारी स्तंभ अभिलेख में उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम के समय में पुष्य मित्रों तथा संभवत हूणों के साथ भी स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन है।इस अभिलेख से स्कंद गुप्त के कार्यकलापों का वर्णन प्राप्त होता है बताया गया है कि उसने आक्रमणकारी या आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया और विजई होकर वापस राजधानी लौट आया प्रतीत होता है कि उसके वापस लौटने पर उसके पिता ने राज्य कार्य उसे सौंप दिया। इनके अलावा मोहरे भी गुप्तकालीन जानकारी प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है।इतिहासकारों का यह मानना है कि अगर किसी देश का इतिहास जानना है तो उसके तत्कालीन सिक्कों का प्रचलन देखना चाहिए भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाला वंश का इतिहास उसके सिक्के के रूप में दिखाई देता है गुप्त वंश के सिक्के बहुमूल्य धातु जैसे सोने और चांदी के अलावा शीशे के बने होते थे विदेशी व्यापार की अधिकता के कारण सोनभंडार में हमेशा वृद्धि होती रहती थी और इस कारण समाज में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन अधिक था।गुप्त वंश में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अधिक था इसके अतिरिक्त इस मुद्रा में कलात्मकता का भी अधिक किया था उस समय जारी की गई स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था इन मुद्राओं के निर्माण में कुषाण वंश द्वारा प्रयोग की गई स्वर्ण मुद्रा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम थी ।
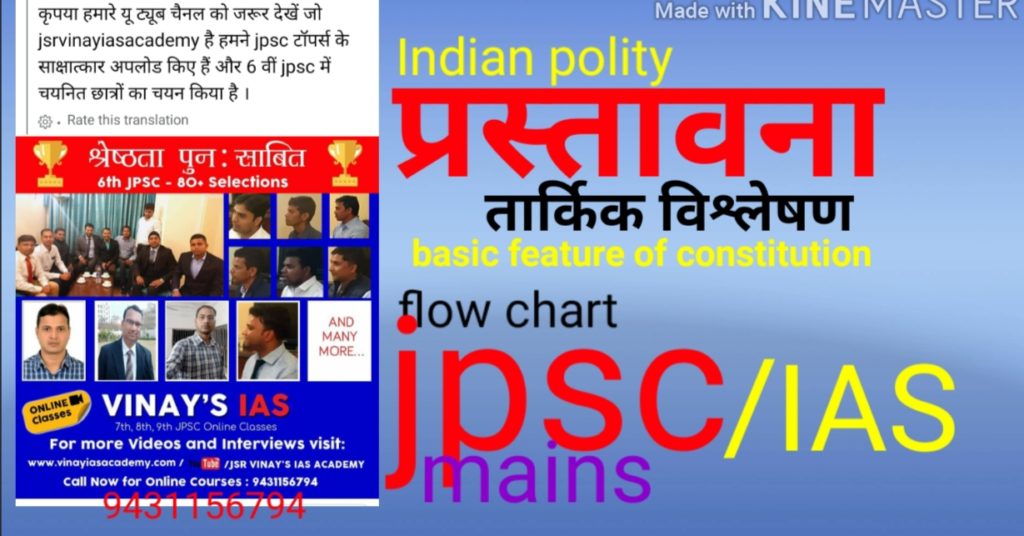
इसके अलावा जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन कर लिया तब विजय प्रतीक स्वरूप चांदी के सिक्के जारी किए गए लेकिन यह मुद्रा आम आदमी के दैनिक व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं थी इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें वस्तुओं के आदान-प्रदान और कौड़ियों का प्रयोग से काम चलाना पड़ता था।गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था इन सिक्कों के एक और चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था तो दूसरी और रानी कुमार देवी को अंकित किया गया था अपने पूरे शासनकाल में चंद्रगुप्त ने इस प्रकार के छह सिखों को जारी किया था आरंभ में इन सिक्कों का वजन 120 से 121 ग्रैंन हुआ करता था।चंद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों में सबसे अधिक प्रचलित सिक्कों में हुआ सिक्का था जिसमें उसके बाएं हाथ में ध्वज धारण किए हुए था इस चित्र में भी उसके कुषाण सम्राट की भांति विदेशी पोशाक धारण किए हुए दिखाया गया है इसी प्रकार चंद्रगुप्त की रानी को भी विदेशी रूप में दिखाया गया था।चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिखों में विदेशी कोर्ट नहीं था समुद्र ग्रुप में अपने सिक्कों में स्वयं को एक धनुर्धर के रूप में प्रदर्शित किया था इस चित्र को आगे आने वाले गुप्त शासकों ने भी पसंद करते हुए अपनाया था इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिखों में उसे एक हाथ में युद्ध में प्रयोग किए जाने वालेकुल्हाड़ी के साथ भी दिखाया गया है और इसके साथ ही उसके सामने एक संदेश वाहक अभी खड़ा है समुद्रगुप्त ने कला प्रेमी व धार्मिक रूप को भी सिखों के रूप में दिखाया जा सकता है कुछ सीखो मैं उसे वीणा बजाते हुए यज्ञ करते हुए भी दिखाया गया था समुद्रगुप्त ने मुख्य रूप से केवल 10 शिक्षकों को ही जारी किया था उसके राज्य में तांबे के सिक्के का प्रचलन नाममात्र का ही था इस समय जारी किए गए सिक्के का वजन 144 ग्रेन था जबकि चांदी के सिक्कों का भार 30336 ग्रेन रखा गया था।गुप्त वंश के एक और शासक कुमारगुप्त ने भी कुछ सिक्कों को जारी किया था यह सिक्के पहले के शासकों की तुलना में काफी भीड़ थी कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में लगभग 14 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था इन सिक्कों में अधिकतर घुड़सवार की आकृति वाले सिक्के देखे जा सकते हैं।इसके अलावा नाचते हुए मोर को भी कुछ स्वर्ण मुद्रा में अंकित किया गया था अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए कुमारगुप्त ने स्वयं को एक अधिकारी व क्षत्रिय के रूप में भी सिखों पर अंकित करवाया था इसके लिए कहीं चीते का शिकार तो कहीं अश्वमेघ करते हुए अंकित करवाई गई इसके अतिरिक्त को सिखों पर देखा जा सकता है चंद्रगुप्त भाटी राजा रानी को भी सिखों पर अंकित करवाया गया इस प्रकार कहा जा सकता है गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का परिचायक रहे हैं।मुजफ्फरपुर जिले में वैशाली से बहुत बड़ी संख्या में मोरे प्राप्त हुई है चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी महादेवी ध्रुवस्वामिनी की मुहर भी प्राप्त हुई है यह महाराजा गोविंद गुप्त की माता की यह संभवत कुमारगुप्त प्रथम का छोटा भाई था अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में हुआ वैशाली का गवर्नर था वैशाली के अन्य कर्मचारियों की अनेक मोरे भी वहां से प्राप्त हुई है मोरो की विविधता तथा नमूने से प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन के संबंध में पता चलता है उच्च तथा अधीन कर्मचारियों की मोहरे प्राप्त हुई है नागरिक तथा सैनिक प्रशासन ने कर्मचारियों की एक लंबी सूची हमें प्राप्त हो जाती है। गोपी इतिहासकार की बहुत सी सामग्री गुप्त सम्राटों के सिक्कों से प्राप्त होते हैं गुप्त वंश के सिक्कों का नियमित अध्ययन किया गया है समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के प्राप्त हुए हैं इन पर चंद्रगुप्त प्रथम तथा उसकी रानी कुमार देवी के चित्र अंकित है। समुद्रगुप्त के चीता प्रकार वीणा वादक प्रकार और श्रमिक प्रकार पताका प्रकार धनुर्धर प्रकार आदि सिक्के प्राप्त हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के भी विभिन्न प्रकार के अनेक सिक्के हैं यथा धनुर्धर प्रकार संघ प्रकार छात्र प्रकार शेर घातक प्रकार घुड़सवार प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के भी कई सिक्के मिले हैं जो धनुर्धर प्रकार अशोक में प्रकार घुड़सवार प्रकार से घातक प्रकार चीता घातक प्रकार हाथी सवार प्रकार आदि स्कंद गुप्त के धनुर्धर प्रकार के सिक्के मुख्यतः सोने के हैं इसको मुद्रा लेखों से कवि की श्रेष्ठ झलकती है चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के केवल उन्हीं प्रदेशों के लिए चलाएं जो पहले पश्चिमी क्षेत्र को के अधीन किंतु बाद में चांदी के सिक्के ग्रुपों के लिए भी चला दिए गए।




