वस्त्र उद्योग– भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान लगभग 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में 4% है जबकि विदेशी आय में 13.5% है। यह 3:30 करोड़ बेटियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा इसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति यों और महिलाओं की है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है इसलिए इस उद्योग की वृद्धि और विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पिछले छह दशकों की तुलना में आज भारतीय वस्त्र उद्योग मजबूत स्थिति में हैं। पिछले 4 दशकों से इस उद्योग में 3 से 4% का विकास हो रहा था लेकिन आज इसकी सालाना विकास दर 8:00 से 9% हो गई है। भारत का कब वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है इसका भारत के निर्यात में 13.5% का योगदान है भारतीय वस्त्र उद्योग तकनीकी पिछड़ेपन का भी सामना कर रहा है इसके अलावा कुशल श्रम शक्ति की भी कमी हो रही है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र उद्योगः
सूती वस्त्र उद्योग– सूती वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश के सर्वाधिक व्यापक रूप से वितरित उद्योगों में से एक है तथा इसमें देश के कुल औद्योगिक क्रम का पांचवा हिस्सा शामिल है अधिकांश सूती वस्त्र मिले अभी भी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थित है। पहला सूती वस्त्र मिल 1854 ईसवी में कवासजी टावर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में करीब 1846 सूती वस्त्र मिले हैं। वस्त्र का सर्वाधिक खाना खाना महाराष्ट्र में है जिसके प्रमुख केंद्र हैं सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और जलगांव। अमेरिका और चीन के बाद भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है तथा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग मैं सम्मिलित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं।

रेशमी वस्त्र उद्योग– प्रथम रेशम वस्त्र उद्योग की स्थापना 1832 ईसवी में हावड़ा में की गई। भारत कच्चे रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल रेशम उत्पादन का 18% उत्पादन भारत में होता है। कर्नाटक देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चार प्रकार के रेशम मलबाड़ी, टसर, एरी और मूंगा पाए जाते हैं। मूंगा सिल्क उत्पादन में विश्व में भारत को एक अधिकार प्राप्त है जो कि आसाम में होता है। देश में रेशम बनाने तथा कपड़ा तैयार करने के कुल 300 कारखाने हैं जम्मू-कश्मीर में रेशमी वस्त्र तैयार करने के 80 छोटे-छोटे कारखाने हैं तथा श्रीनगर में रेशम का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है।
ऊनी वस्त्र उद्योग– भारत में आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत 18 से 76 ईसवी में कानपुर में लाल इमली द्वारा किया गया था। 1835 ईस्वी में धारीवाल तथा मंगलौर में ऊनी मिल की स्थापना की गई। ऊनी वस्त्र उद्योग के करीब 50% मिले पंजाब में है तथा उत्पादन के मामले में विश्व में भारत नवम स्थान पर है।
चीनी उद्योग- चीनी उद्योग सर्वाधिकउत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु तथा कर्नाटक राज्य में है। गन्ने से चीनी आदि बनाने का काम तो भारत में ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही प्रचलित रहा है किंतु आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का वर्तमान उद्योग इसी शताब्दी की देन है। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान ब्राज़ील के बाद विश्व में दूसरा है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार के बेतिया में 1840 ईसवी में की गई। देश में चीनी की सर्वाधिक मिले महाराष्ट्र में स्थित है। 1995 में भारत में 435 कारखाने थे जिनकी स्थापना मुख्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों या उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही की गई थी क्योंकि गन्ना शीघ्र ही सूख जाता है इसलिए इसको शीघ्रता से कारखानों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है। वर्तमान में देश में चीनी मिलों की संख्या 642 है। देश में सर्वाधिक गन्ना चीनी और गुड उत्पादक उत्तर प्रदेश है।

शीशा उद्योग- भारत का पहला शीशा कारखाना 1941 इसी में खोला गया। भारत में शीशा उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। भारत में शीशा उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद है। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है।
दवा निर्माण उद्योग – स्वास्थ्य दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में सर्वोपरि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यही कारण है कि दवा उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्योग के रूप में देखा जाता है। भारतीय दवा उद्योग वैश्विक फार्मा सेक्टर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास भी हुआ है। विश्व में अलग-अलग बीमारियों की 50% टीको की मांग भारत से पूरी होती है। अमेरिका में सामान्य दबाव की मांग का 40% और ब्रिटेन की कुल दवाओं की 25% आपूर्ति भारत में निर्मित दवाओं से ही होती है। इसके अलावा विश्व भर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए प्रयोग की जाने वाली एंट्री रेट्रोवायरल दवाओं की 80% आपूर्ति भारतीय दवा कंपनियां ही करती हैं। 2020 तक भारतीय दवा उद्योग वृद्धि के मामले में विश्व के शीर्ष तीन दवा बाजारों और आकार के मामले में विश्व का सबसे अच्छा सबसे बड़ा बाजार भारत होने वाला है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 ईस्वी में पिपरी के पुणे में की गई थी ड्रग एवं फार्मर क्यूटिकल्स के क्षेत्र में यह देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। भारतीय औषधि एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई जिसका 3 केंद्र ऋषिकेश, गुड़गांव तथा हैदराबाद में है।
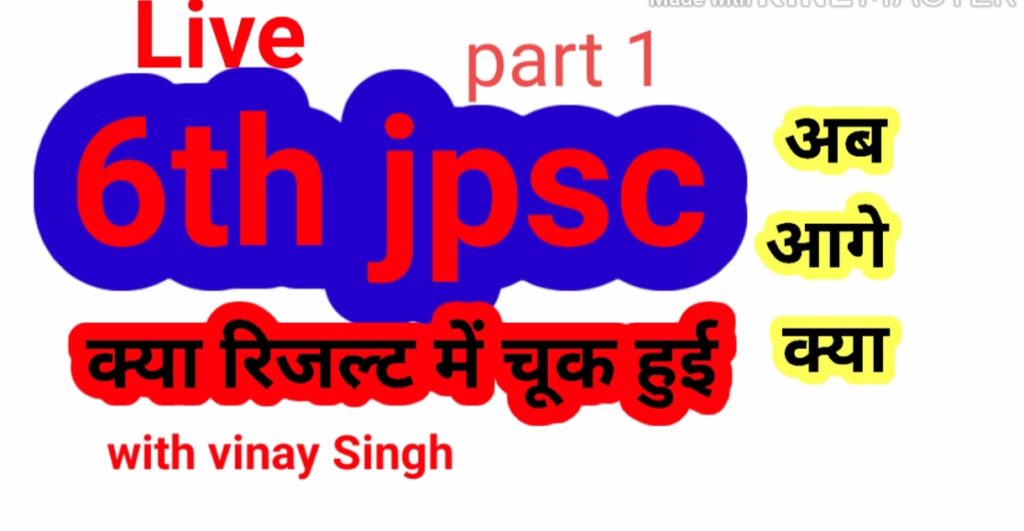
रसायनिक खाद उद्योग– भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। भारत पोटाश उर्वरक के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है। 1986 में तमिलनाडु के रानी पेट में सुपर फास्फेट बनाने का कारखाना खोला गया । कर्नाटक के बेलागुला में 1939 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का कारखाना खोला गया। 1951 ईस्वी में झारखंड के सीनरी में उर्वरक उत्पादन का प्रथम सरकारी कारखाना खोला गया। सिंदरी उर्वरक संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है। देश के शीर्ष उर्वरक उत्पादक राज्य गुजरात, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश राष्ट्र हैं। नाइट्रोजन खाद बनाने में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।
इस तरह के सारे उद्योग धंधों से भारत परिपूर्ण है जो कि भारत में बेरोजगारी को कम करता है इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपना संपूर्ण योगदान इसे विकसित करने में दें।




